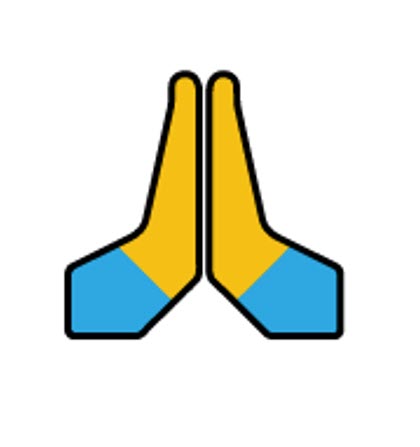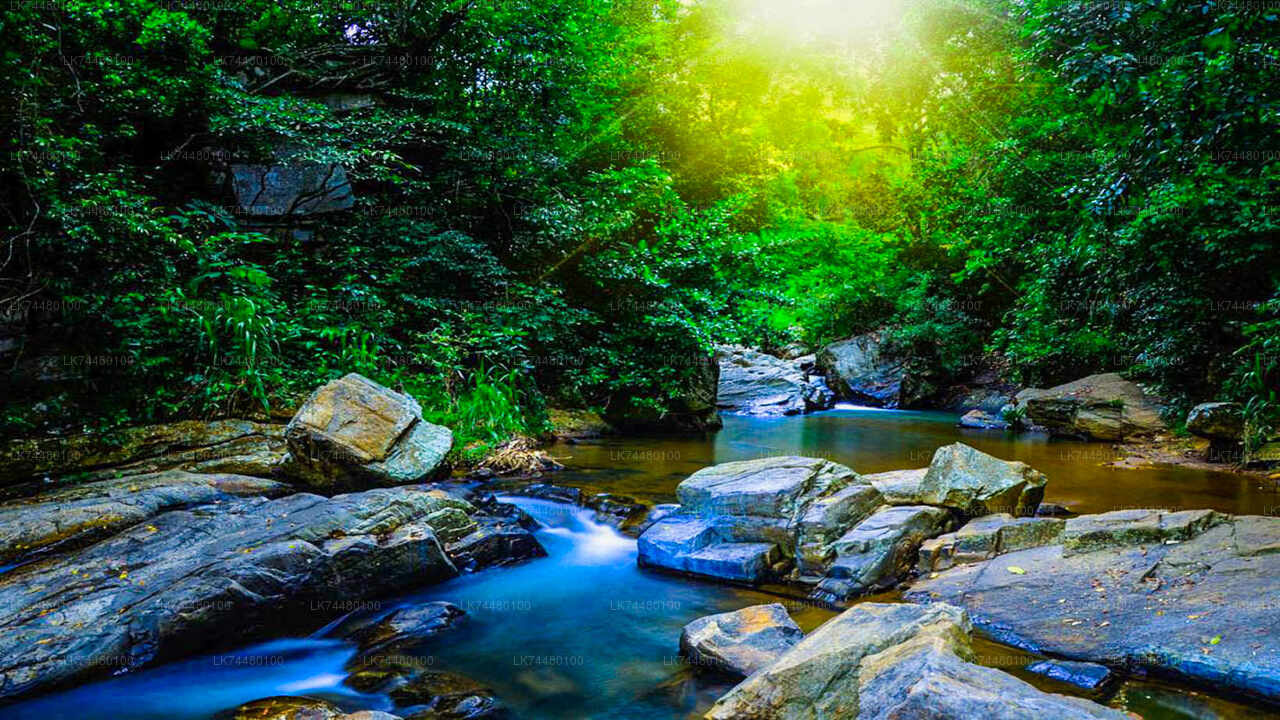रत्नापुरा शहर
रत्नापुरा को श्रीलंका के "रत्नों के शहर" के रूप में जाना जाता है, जो रत्न खनन और व्यापार का केंद्र है और द्वीप के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह कालू नदी के किनारे, एडम्स पीक की तलहटी में, हरे-भरे परिदृश्यों से घिरा हुआ है और सांस्कृतिक अनुभवों और क्षेत्र के प्रसिद्ध कीमती पत्थरों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक केंद्र है।
बालंगोडा मैन

श्रीलंका को मानव विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बाटाडोम्बालेना गुफाएँ रत्नापुरा में स्थित हैं और यहाँ मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं, जिनमें एक प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी भी शामिल है। विस्तृत अनुसंधानों और अभियानों ने हमारे पूर्वजों के जीवन-शैली से संबंधित नई जानकारियाँ उजागर कीं। इसे मानव विकास के अध्ययन में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है।
बालानगोड़ा मानव (බලංගොඩ මානවයා), Homo sapiens balangodensis, मेसोलिथिक काल में रहने वाला सबसे प्राचीन ज्ञात मानव है। स्रोतों के अनुसार, बालानगोड़ा क्षेत्र के पास एक पुरातात्विक स्थल पर एक कंकाल मिला था। खोज के स्थान के आधार पर इसे "बालानगोड़ा मानव" नाम दिया गया।
गुफाओं और अन्य स्थलों पर मिले प्रमाणों के अनुसार, बालानगोड़ा मानव लगभग 38,000 वर्ष पूर्व दिखाई दिया। हाल में खोजी गई हड्डियों से पता चलता है कि कुछ अवशेष लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। यह इस बात का पहला प्रमाण है कि आधुनिक संरचना वाले मानव उस समय दक्षिण एशिया में मौजूद थे। कंकाल के साथ, सांस्कृतिक अवशेष भी पाए गए, जिनमें ज्यामितीय माइक्रोलिथ शामिल थे, जो 28,500 वर्ष पुराने हैं। पत्थर के औज़ारों के उपयोग का सबसे पुराना प्रमाण इसी स्थल और कुछ अफ्रीका के स्थलों से मिलता है।
बालानगोड़ा मानव
बालानगोड़ा मानव कद में लंबा था और दसियों हज़ार वर्ष पहले रहता था। यह प्राचीन होमिनिड पुरुष लगभग 174 सेंटीमीटर और महिलाएँ लगभग 166 सेंटीमीटर लंबे थे। अध्ययन और अभियानों ने हमारे प्राचीन पूर्वजों की जीवनशैली के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की है।
अध्ययनों के अनुसार, प्राचीन मनुष्यों की नाक धँसी हुई होती थी, उभरी भौंह की हड्डियाँ, मोटी खोपड़ी, बड़े दाँत, छोटी गर्दन और मजबूत जबड़ा होता था। गुफाओं में मिले मानव अवशेष लगभग 16,000 वर्ष पुराने हैं। विश्लेषण से इनके जैविक गुणों में उल्लेखनीय समानताएँ मिलीं।
अनुसंधान से आधुनिक श्रीलंकाई मूलनिवासी वेड्डा जनजाति से प्राकृतिक संबंध होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बसे बालानगोड़ा मानव बाद में मैदानी इलाकों में चले गए और शिकार से कृषि की ओर बढ़े।
बेलनबंडी पालासा में हाथी की टांग की हड्डियों से बने मेसो-नियोलिथिक औज़ार मिले हैं। साथ ही हिरण के सींगों से बने चाकू और औज़ार भी मिले हैं। अन्य स्थलों में ओखर (लाल मिट्टी), पालतू कुत्तों, दफ़न स्थलों और आग के बड़े पैमाने पर उपयोग के प्रमाण मिले हैं।
अन्य रोचक अवशेषों में व्यक्तिगत आभूषण और भोजन के अवशेष शामिल हैं — जैसे सीपियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, शार्क की कशेरुकाओं से बने मोती, सीपियों के लटकन, हड्डियों से बने उपकरण, जंगली केले और ब्रेडफ्रूट के अवशेष आदि।
समुद्री सीपियों और शार्क दाँतों का बार-बार मिलना यह संकेत देता है कि गुफाओं में నివास करने वालों का तट से सीधा संपर्क था, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर था। बेली लेना से मिले प्रमाण बताते हैं कि नमक तट से गुफा तक लाया जाता था।
ज़्यादा गतिशीलता, वर्षावन संसाधनों का उपयोग और मौसम व पर्यावरण के बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता माइक्रोलिथिक परंपरा के साथ पाई जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हॉर्टन प्लेन्स में मिले ज्यामितीय माइक्रोलिथ बताते हैं कि यह क्षेत्र मेसोलिथिक काल में आबाद था।
निम्न-भूमि के शिलाश्रयों में रहने वाले शिकारी-संग्रहकर्ता संभवतः अपने वार्षिक भोजन चक्र के दौरान शिकार और जंगली अनाज एकत्र करने के लिए हॉर्टन प्लेन्स आते थे। हॉर्टन प्लेन्स एक अस्थायी कैंप स्थल के रूप में उपयोग होता था।
जंगली ब्रेडफ्रूट, केला, और अन्य वनस्पतियों का उपयोग देर प्लेइस्टोसीन और प्रारंभिक होलोसीन में किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में शिकारी-संग्रहकर्ता से किसानों की ओर परिवर्तन शुरू हो गया था। माना जाता है कि कृषि शुरू करने के लिए मानव ने जलाकर खेती (स्लैश एंड बर्न) के तरीके का उपयोग किया।
बालानगोड़ा मानव का इतिहास
आधुनिक मानव आचरण और मानव विस्तार का इतिहास दक्षिण एशिया के देर प्लेइस्टोसीन काल की पुरातात्विक सामग्री से जुड़ता है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व, पॉक जलडमरूमध्य और एडम्स ब्रिज डूबने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका के बीच भूमि-पुल मौजूद था, जिसके जरिए मानव और जानवर यात्रा कर सकते थे।
पैलियंटोलॉजिस्ट्स ने हंबनटोटा जिले में लगभग 125,000 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक जीव-जंतु के अवशेष पाए, बुंडाला के समीप। यहाँ क्वार्ट्ज और चर्ट (सिलिका पत्थर) से बने औज़ार भी मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रारंभिक मानव 300,000 से 500,000 वर्ष पूर्व ही श्रीलंका में रह रहे थे।
दक्षिण एशिया भर में प्रारंभिक मानव बसाहट के अनेक प्रमाण मिले हैं। भारत में 200,000 वर्ष पुराने मानव की खोपड़ी मिली, जिसे "नर्मदा मानव" कहा गया। यद्यपि यह आधुनिक मानव नहीं था, यह दक्षिण एशिया में मानव अस्तित्व का पहला प्रमाण माना जाता है।
खोज के बाद उसकी टैक्सोनोमिक पहचान को लेकर विवाद हुआ। 1955 में, दारनियागला ने “Homo sapiens balangodensis” नाम प्रस्तावित किया।
बालानगोड़ा मानव के प्रमाण
लगभग 40,000 वर्ष पुराने श्रीलंका के जीवाश्म रिकॉर्ड पहले की अपेक्षा बहुत अधिक संगठित हैं। दक्षिण एशिया में आधुनिक मनुष्यों के पहले प्रमाण इसी काल के हैं।
कालुतारा में स्थित "फा-हियेन गुफा" में सबसे पुराने मानव जीवाश्म मिले हैं। यह गुफा प्राचीन चीनी भिक्षुओं द्वारा बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती थी। कार्बन डेटिंग से साबित हुआ कि गुफा 34,000 से 5,400 वर्ष पहले तक आबाद थी।
श्री पादा (एडम्स पीक) क्षेत्र में बाटाडोम्बा लीना गुफा प्रणाली से कई मूल्यवान प्राचीन कलाकृतियाँ मिलीं।
1930 के शुरुआती उत्खननों में बच्चे और कुछ वयस्कों की हड्डियाँ मिलीं। 1981 में और अधिक अवशेष मिले, जिनकी आयु 16,000 वर्ष बताई गई। अगले वर्ष माइक्रोलिथ और चारकोल के नमूने मिले, जिनकी आयु लगभग 28,500 वर्ष थी।
किटुलगाला और बेली लेना की गुफाओं में और बुंडाला के दो तटीय स्थलों में मिले माइक्रोलिथ विश्व के सबसे पुराने माइक्रोलिथ में से हैं — अफ्रीका के माइक्रोलिथ के समान। भारत में यह तकनीक लगभग 24,500 वर्ष पहले उपयोग में आई।
सबारागमुवा और ऊवा क्षेत्रों में मिले प्रमाण बताते हैं कि माइक्रोलिथिक तकनीक लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व तक जारी रही। बाद में इसे बड़े पत्थर के औज़ारों से बदला गया।
बेली लेना गुफा और बेलनबंडी पालासा में भी मानव हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कार्बन विश्लेषण से सिद्ध हुआ कि इस अवधि में श्रीलंका निरंतर आबाद था।
वेड्डा जनजाति से संबंध
ऐतिहासिक अभिलेख श्रीलंका के मूल निवासियों "वेड़्दा" को शिकारी-संग्रहकर्ता बताते हैं, जो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। वे शहद और शिकार को पास के गाँवों से धातु के औज़ारों के बदले में विनिमय करते थे। दारनियागला के अनुसार, बालानगोड़ा मानव वेड्डा और कुछ सिंहली समूहों का प्रत्यक्ष पूर्वज है।
समय के साथ कुछ वेड्डा लोग गाँवों में रहने लगे या कैंडी राज्य में सैन्य दलों में शामिल हुए।
वेड़्दा लोगों के कद छोटे, खोपड़ी मजबूत, दाँत बड़े और उनकी अनुवांशिक विविधता अधिक पाई गई है। आनुवंशिक अध्ययनों के अनुसार, वेड्डा लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंहली और श्रीलंकाई तमिलों से अधिक मेल खाता है बजाय भारतीय तमिलों के।
संभावना है कि बालानगोड़ा मानव के कुछ गुण अभी भी आज के श्रीलंकाई लोगों में पाए जाते हैं।
माना जाता है कि बालानगोड़ा मानव 500 ईसा पूर्व तक जीवित था और संभवतः वर्षावनों में इससे भी अधिक समय तक रहा। भारतीय प्रवासियों के आगमन के साथ इनकी जनसंख्या धीरे-धीरे कम होती गई।